एक शानदार हड़ताल के असर में निहित संदेश और सबक
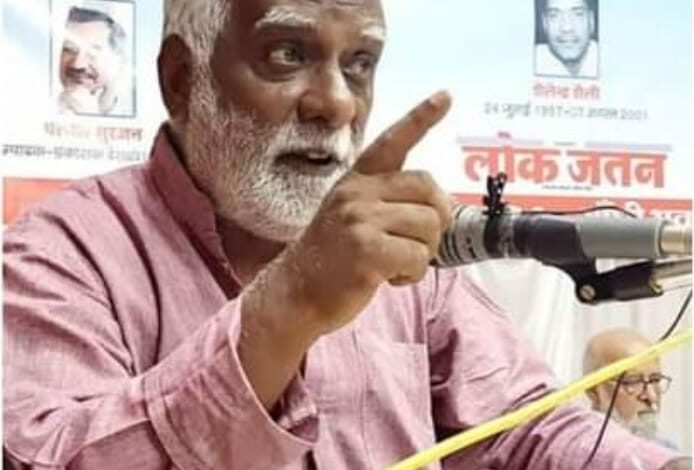
बादल सरोज
9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में कोई 25 करोड़ हिन्दुस्तानियों की भागीदारी ने उसे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लिए भी एक बेमिसाल बड़ी कार्यवाही बना दिया है। दुनिया में कुल अस्तित्वमान 205 देशों में से सिर्फ 5 को छोड़कर किसी भी देश की इतनी आबादी भी नहीं है, जितने लोग 9 जुलाई को भारत में हड़ताल पर गये। महाशक्ति होने का दंभ पाले ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी — इन तीनों देशों की कुल आबादी का जोड़ भी उतना नहीं है, जिससे अधिक लोग 9 जुलाई को हड़ताल पर थे। यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी वाली हड़ताल थी, मगर कोई पहली हड़ताल नहीं थी। नीतियों की दुर्गन्ध मारती नालियों और गटरों को मूंदने-पाटने के लिए ऐसी कामयाब हड़तालें और कारगर विरोध कार्यवाहियां तभी से जारी है, जब से इनकी नई और संहारक खेपों की शुरुआत 1991 में आये नवउदारवादी निज़ाम के साथ हुई थी। इसके साथ आयी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के त्रिशूल के खिलाफ इन 34 वर्षों में यह 21 वीं देशव्यापी आम हड़ताल थी। उद्योग और क्षेत्रवार राष्ट्रीय हड़तालों को भी जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या सैंकड़ों में पहुच जाती है। यह तय है कि संघर्ष आगे भी जारी रहेगा – बल्कि उत्तरोत्तर तीव्र ही होगा, क्योंकि ज़ुल्म, अन्याय और वंचना के खिलाफ लड़ना मनुष्य का स्वभाव है। इन संघर्षों ने ही मनुष्य समाज को बनाया है, उसे जितना भी बन सका, मानवीय और सभ्य बनाया है। इस जद्दोजहद का अभिनंदन है और इसमें शामिल होने वाले, इनके साथ अपनी संबद्धता प्रदर्शित करने वाले धन्य हैं ; उन्होंने अपने इंसान होने का परिचय दिया है। ये पंक्तियाँ इस हड़ताल पर नहीं, इसके असर और उनमें निहित संदेश और सबक पर केन्द्रित हैं।
इस इतनी बड़ी कार्यवाही के प्रति इस देश के कथित मुख्यधारा मीडिया का रुख या तो इसकी पूरी तरह अनदेखी करने का था या इसे पूरी तरह असफल बताने का था। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। पिछले तीन दशक में आमतौर से और गुजरे एक दशक में खासतौर से मीडिया पर उन कार्पोरेट्स का सम्पूर्ण वर्चस्व कायम हो चुका है, जिनके खिलाफ यह हड़ताल थी। खुद के मारे जाने का तरीका खुद ही बताने वाले भीष्म पितामह सिर्फ पौराणिक कथाओं या महाकाव्यों में ही होते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं, पूँजीवाद में तो कतई नहीं। यूं भी वर्गीय समाज में मीडिया हो या तंत्र, शासन हो या प्रशासन, उसका घुटना पेट की तरफ मुड़ने के लिए बना है।
मगर इस बीच बात इससे थोड़ा आगे बढ़ी है और सत्तासमूह के इस अतिआत्मविश्वास में बदल गयी है कि भले कितनी हड़तालें और आन्दोलन हो जाएँ, उसके राज पर कोई आँच नहीं आने वाली। उसे इस बात का यकीन है कि वह अपनी तिकड़मो, झांसों, चालों और भुलावों से इस सारे गुस्से को यदि काफूर न कर सका, तो उसकी दिशा तो बदल ही देगा और इस तरह हुकूमत में बना रहेगा। यह उसकी आज की आजमाई विधा नहीं है – मानव समाज में जब से राज्य अस्तित्व में आया है, तब से ही राज करने वालों ने यह कला अपनाई है और धीरे-धीरे उसमे पारंगतता हासिल कर ली है। ऐसा नहीं है कि इसका ज्ञान सिर्फ उसे ही है। जिन विचारकों और योद्धाओं ने चंद मुट्ठी भर लोगों के समूह के विराट जनता पर राज करने वाली प्रणाली के रहस्य को समझा, इसको बदलने का रास्ता खोजा, सुझाया और व्यवहार में उतारा, वे भी इसे जानते थे। उन्हें पता था कि मानव समाज में सामाजिक रिश्तों, सामाजिक-राजनीतिक जीवन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है और यह अपने आप या अनायास नहीं आती। अवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का रूप पैदावार की ताकतों के विकास के साथ और उसके नतीजे में लेती है। उन्होंने कहा कि इस विकास और बदलाव का आधार उत्पादन की प्रणाली है। यही निर्णायक है। मगर इस निर्णायक यथार्थ को उन्होंने यांत्रिक तरीके से नहीं लिया, उसकी द्वन्द्वात्मकता को भी पकड़ा। उन्होंने कहा कि पैदावार की प्रणाली सिर्फ उत्पादन ही नहीं करती, इसके आधार पर तत्कालीन समाज के दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक विचार भी बनते और आकार लेते हैं, विचारधारा भी आती है और इसी ढांचे पर खड़ी होती है।
कार्ल मार्क्स ने इसे आधार और ऊपरी संरचना – बेस और सुपर स्ट्रक्चर – के रूप में परिभाषित भी किया, इनकी भिन्नता और पारस्परिकता को भी व्याख्यायित किया। उन्होंने जो मार्के की बात कही वह यह थी कि आधार पर खड़ी संरचना सिर्फ उस पर खड़ी नहीं रहती ; वह इसके साथ अंतर्क्रिया भी करती है। मतलब वह इसे प्रभावित भी करती है। इसकी पुष्टि कई तरह से, हर तरह से हुयी है ; दुनिया में अलग-अलग अवस्थाओं की स्थिति में इसने अलग-अलग तरह से भूमिका निबाही है। शोषकों ने अपने से हजारों गुना बड़ी शोषितों की आबादी के लिए इसी संरचना का सहारा लिया है। एक और असाधारण विचारक, फासीवादी दौर के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तकर ग्राम्शी ने इसे शासक वर्गों द्वारा अपने विचार का प्रभुत्व और वर्चस्व कायम करने और उसका राज चलाने के लिए इस्तेमाल करने के रूप में पहचाना था। खुद मार्क्स ने इसे सपाट तरीके से बयान करते हुए कहा था कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली सिर्फ लोगों के लिए माल ही पैदा नहीं करती, वह अपने माल के लिए लोग भी पैदा करती है। दुनिया भर की शोषक राजसत्ताओं ने यही किया है, भारत में भी यही किया जा रहा है ; अपने माल – हर तरह के माल – के लिए लोग पैदा किये जा रहे हैं। सूचना के क्षेत्र में हुई तकनीकी क्रांति ने उनके इस काम को और आसान बना दिया है।
असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, मेहनतकशों की एकता को नष्ट-भ्रष्ट कर देना, गुस्से को इधर-उधर धकेल देना, अतीत के प्रेतों को जगाकर समाज को उन सब बातों के लिए उन्मादी बना देना, जिनका उसकी जिन्दगी और मनुष्यता की बेहतरी से कोई सीधा ताल्लुक ही नहीं है, इसी तरह की आजमाईशें हैं। दुनिया और भारत का जो प्रभु वर्ग है, वह तुलसी के पद “जा को प्रभु दारुण दुःख देई, ताकी मति पहले हर लेई” पर अक्षरशः अमल कर रहा है। बेहद व्यवस्थित तरीके से आम जन मानस से उसका विवेक छीन रहा है। उसे पाशविकता और अमानुषिकता सिखा ही नहीं रहा, अब तक का सारा सीखा हुआ भुला भी रहा है। मोदी के नए इंडिया में सबसे प्रमुख नया यही है। ऊपर लिखे को दोहराते हुए कहें, तो अपने अनुकूल लोग भी तैयार कर रहा है, अपने लिए सुरक्षित समाज भी बना रहा है।
उसे भरोसा है कि हड़ताल करके गुस्से में नारे लगाती यह भीड़ जलूस और सभाओं के खत्म होने के बाद जैसे ही अलग-अलग मनुष्य के रूप में ठीये लगेगी, अपने घर पहुंचेगी, वह उन्हें दबोच लेगा। उसके घर में लगा टीवी, सुबह आने वाला अखबार, जेब में रखा मोबाइल और कोई कथावाचक उसके बिना जाने ही उसे घसीट कर फिर से उस एजेंडे की कीच में डुबो कर उसका सारा क्रोध, आक्रोश और क्षोभ ठंडा कर देंगे। उसे ऐसे कृत्रिम और काल्पनिक संसार में पहुंचा दिया जाएगा, जहां अम्बानी और अडानी उसे नजर ही आना बंद हो जायेंगे और असली ख़तरा उस असलम और अय्यूब में दिखने लगेगा, जो उसी जैसी या उससे भी बदतर जिन्दगी जी रहे हैं और कुछ घंटा पहले उसी के साथ मुट्ठियाँ ताने नारे लगा रहे थे। उसके हाथ में झंडे की जगह त्रिशूल थमा दिया जाएगा ; आपस में एक-दूसरे में घोंपने के लिए। बात यहीं तक नहीं रुकेगी ; धर्म और मजहब की दीवारों की चौहद्दियों के भीतर भी उसे अपना-पराया ढूँढने तक पहुंचाएगी। शुरुआत ‘मेरी जात तेरी जात’ से होगी, उसके बाद एक ही जाति में ‘मेरे गोत्र तेरे गोत्र’ तक जायेगी। अंत में घर की देहरी लांघ कर अन्दर आकर आदमी और औरत के अलगाव और उनमें छोटे-बड़े की खाइयाँ गहरी करते हुए अंततः उसे एकदम तनहा करके ही मानेगी। पता नहीं तब भी मानेगी कि नहीं मानेगी!!
सता पर काबिज गिरोह आश्वस्त है कि ऐसा करते हुए इस गुस्से के असर को वह बेअसर कर देगा और सच्ची बात यह है कि उसकी यह आश्वस्ति निराधार नहीं है। ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद हुए चुनावों में इस आन्दोलन के केंद्र रहे दिल्ली के सीमावर्ती प्रदेशों में भाजपा की जीत और बढ़त इसका उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में दसियों लाख की रैलियों और साल दर साल, हर सप्ताह-महीने जनमुद्दों पर हो रहे मैदानी संघर्ष के बाद भी आखिर में ईवीएम की मशीनों पर अँगुलियों का रास्ता भटक जाना इसी की मिसाल है।

सबक यह है कि जिन तरीकों, माध्यमों से हुक्मरान अवाम की ऐसी शानदार कार्यवाहियों के असर से खुद को महफूज रखना चाहते हैं, रखते हैं, उन्हें समझ कर, उनकी काट करके, उन्हें भोंथरा करके ही इन कार्यवाहियों की कारगरता बढ़ाई जा सकती है। यह काम प्रतिरोधात्मक और प्रतिबंधात्मक – मेडिकल साईंस की भाषा में कहें, तो क्यूरेटिव और थेरेपेटिक – दोनों तरह से करना होगा। भ्रांतियों की धूल की धुलाई भी करनी होगी, वे जिस कूड़े में वे पनपती हैं, उसकी सफाई भी करनी होगी। निस्संदेह हड़ताल क्रान्ति के अलावा वर्गीय कार्यवाही का दूसरा सबसे बड़ा रूप है, वर्गीय संघर्ष में मेहनतकश वर्ग की उच्चतर कार्यवाही है। मगर जैसा कि वर्ग संघर्ष को समाज की चालक शक्ति और बदलाव का इंजिन बताने वाले कह गए है ; यह वर्ग संघर्ष सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं होता। विचार, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक जीवन शैली सहित हर उस मोर्चे पर होता है, जिनका मनुष्य के जीवन के साथ रिश्ता है।
इसलिए ऐसी हड़तालें तभी अपनी समग्रता में पहुंचेंगी, तभी पूर्णता हासिल करेंगी, जब वे सत्ता वर्गों के चक्रव्यूह को, उसके हरेक व्यूह को तोड़ने में महारत हासिल करेंगी। दुनिया में जहां-जहां, जब-जब यह हुआ है, वहां-वहां, तब-तब हडतालें हड़तालों तक ही नहीं रुकी हैं, वे क्रांतियों में बदली हैं। बाकी जगह भी ऐसा होना तय है, मगर अपने आप न वहां हुआ था, न यहाँ होगा।




